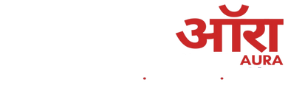ताजमहल, मोहब्बत की ऐसी निशानी जिस पर शायरों ने अपने हुनर आज़माए, चित्रकारों ने अपनी कला को कैनवास पर उकेरा, फिल्मकारों ने अपनी महारत को परदे पर उतारा. गीतकारों ने नग़मे लिखे, संगीतकारों ने सुर सजाए, फोटोग्राफ़रों ने संगतराश की कलाकारी को समय और स्थान की कैद से आज़ाद किया और स्थापत्य कला की बारीकियों को दुनिया के कोने-कोने तक पहुंचाया. लेखकों ने इसे शब्दों के मोती की माला में पिरोया और इतिहासकारों ने इसे वक़्त की अमानत के रूप में दर्ज किया. हर दौर की नई पीढ़ियों ने इससे इश्क़ करने का सलीका सीखा.
इस मोहब्बत की निशानी ने इश्क़ के उस रूप से रु-ब-रू कराया, जहां इश्क़ का आख़िरी पड़ाव सब कुछ निछावर करना होता है, खुद का फ़ना हो जाना होता है. वफ़ा के उस उसूल को याद दिलाया, जहां मोहब्बत सिर्फ़ बदन की गिरवी नहीं होती, बल्कि रूहों में उतरने की यात्रा होती है.
यह ताजमहल का ही जलवा है कि तवायफ़ों से लेकर कव्वालों तक, सभी इसकी तारीफ़ के पुल बांधने से खुद को नहीं रोक पाए. तवायफ़ों ने अपनी दास्तानों और महफ़िलों में इसका ज़िक्र किया और अपने क़द्रदानों, मेहरबानों, आशिक़ों से नज़राने वसूलती रहीं. अलग-अलग दौर में बादशाहों ने अपनी शानो-शौकत और इश्क़ की मिसाल पेश करने के लिए इसकी नकल की, लेकिन नाकाम रहे.
चार सौ साल हो गए, लेकिन यह इमारत गुजरती सदियों से आज भी बात करती है. इस दौर में हर तरह के शासक आए और गए- अच्छे भी, बुरे भी. लेकिन ज़्यादातर शासकों ने इसे विरासत और सत्ता की स्मृति के रूप में देखा. आलोचक भी हुए, मगर अधिकतर इस नतीजे पर पहुँचे कि इसे इतिहास और कला की कसौटी पर परखा जाए और जमकर तारीफ़ की. हद तो यह है कि हर नई चीज़ का विरोध करने वाले धर्मावलंबियों ने भी इसे समय और नियति के बीच खड़ी एक निशानी माना. मस्जिद के वायज़ और मंदिर के पुजारी तक- कोई भी इसके विरोध में नहीं उतरा. दुनियाभर के सैलानी इसी इमारत को देखने पूरब की तरफ़ भागते दिखे. उन्होंने ताजमहल को हिंदुस्तान की पहचान और मोहब्बत के प्रतीक के तौर पर जाना.
लेकिन इससे बड़ी विडंबना और क्या होगी कि यह देश नफ़रत के बाज़ार में इस क़दर डूबा कि अब एक मंचीय कवि इसे ‘सफ़ेद कब्रिस्तान’ बता रहा है और उसके बयान के साथ ही हर तरफ़ सन्नाटा है. विरोध के स्वर आए भी तो पारंपरिक विरोधियों की तरफ़ से और बहुत ही सीमित. मंचीय कवि जिस शब्द-परंपरा से आते हैं, शायद उन्होंने नफ़रत के उस दलदल में अपना घर बसा लिया है, जहां अब साफ़, सुंदर और सुगंधित कमल की पौध मुरझा चुकी है. वहां से अब सिर्फ़ गंध आती है… और मुमकिन है कि मंचीय कवि को यही फ़ज़ा रास आ रही हो, ज़्यादा पुरसुकून लग रही हो.

दस्तूर यह है कि जब किसी की आलोचना करें तो कम से कम अपनी परंपरा की कसौटी पर उसे तौलना चाहिए. भारतीय साहित्यिक परंपरा 20वीं सदी में अगर किसी एक शख़्स पर नाज़ कर सकती है, तो वह हैं रवीन्द्रनाथ टैगोर- जिन्होंने अपनी शाहकार नज़्म में लिखा था: “ताज महल समय के गाल पर आँसू की एक बूँद है.”
टैगोर की कविता में अगर खोट है या एक सदी के सफ़र में यह कविता अपनी प्रासंगिकता खो चुकी है, तो कम से कम इसका खुले तौर पर इकरार हो, एलान तो हो. बताया जाए कि टैगोर अपनी रचना में बेमानी बात कह गए. उनकी यह लाइन इतिहास का महज़ कूड़ा बन चुकी है. ताजमहल की अज़मत का इकरार उर्दू के अनेक आलोचक भी करते थे. वे कहते थे कि मुगलों ने भारत को तीन चीज़ें दीं- उर्दू, ग़ालिब और ताजमहल. उर्दू के मशहूर आलोचक गोपीचंद नारंग ने उर्दू की तारीफ़ में इस भाषा की ताबीर ताजमहल से की. उन्होंने कहा था, ‘मैं उर्दू को भारत का भाषाई ताजमहल कहता हूं.’ नारंग ने एक साथ ताजमहल और उर्दू दोनों की तारीफ़ एक लाइन में बयान कर दी. टैगोर, नारंग – ये वो अज़ीम शख़्सियतें हैं जिनके कदमों की खाक भी काबिल-ए-एहतराम है.
साहिर, जो ताजमहल को लेकर कुछ यूं गोया होते हैं –
इक शहंशाह ने दौलत का सहारा ले कर
हम ग़रीबों की मोहब्बत का उड़ाया है मज़ाक़
वही साहिर जब फिल्म ताजमहल के लिए गीत रचते हैं तो फरमाते हैं – “जो वादा किया…” जहां रोशन के संगीत से सजा यह नग़मा रफ़ी की रुहानी, नफ़ासत भरी और दिलकश आवाज़ के जादू और लता की मख़मली और लचकदार सुरों की सजावट से अवाम के बीच आता है, तो हरेक ज़बान पर छा जाता है. यह अमर गीत भी इसी ताजमहल की मरहून-ए-मिन्नत है.
यह सच है कि ताजमहल आलोचना से परे नहीं है. लेकिन आलोचना में नफ़रत हो, ख़ासतौर पर धार्मिक और इसके साथ ही लालच हो, कुछ पाने की उम्मीद हो तो यह समझना मुश्किल नहीं है कि गिरने का सफ़र किस तेजी से तय किया जा रहा है.